Hindi sahitya :भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा के बारे में अनेक सम्प्रदाय प्रचलित हुए हैं। जैसे अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि रस तथा औचित्य सम्प्रदाय।
इनके प्रवर्तक आचार्यों ने भले ही काव्य के मूल तत्त्व के रूप में अलंकार रीति और ध्वनि आदि स्वीकार किये हों किन्तु सभी में आनन्द तत्त्व को मूलतः स्वीकार किया है।
वस्तुतः काव्यास्वादन से प्राप्त आनन्द ही काव्य का मुख्य तत्त्व है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा भी है- "वाक्यं रसात्मकम काव्यम" इस परिभाषा में रस को काव्य का प्राण तत्त्व माना गया है।
उसी से चिर आनन्द की प्राप्ति होती है। यह आनन्द पाठक को अतीन्द्रिय जगत में ले जाता है और सहृदय व्यक्ति उसमें डूब जाता है।
रस की परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है-"विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः।" अर्थात् विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के समुचित मेल से स्थायी भावों का आस्वादन ही रस है।
दूसरे शब्दों में- काव्य के पठन पाठन, श्रवण या दर्शन से पाठक, श्रोता या दर्शक, को जिस आनन्द की अनुभूति होती है, वही रस है।
रस को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। अर्थात् एक साधक को ईश्वरोपासना करते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है वही सहृदय को किसी काव्य का आस्वादन करते समय प्राप्त होता है।
हमारे जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनकी प्रेरणा और लक्ष्य, आरम्भऔर अन्त रस में ही हैं।
रसवादी आचार्यों में आनन्द वर्धन, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दी आचार्यों में रामचन्द्र शुक्ल इसके सर्वश्रेष्ठ पोषक रहे हैं। उन्होंने हृदय की मुक्तावस्था को ही रस दशा की प्राप्ति माना है।
रस हमारी चित्त वृत्तियों को सात्विक बनाता है जिससे मनुष्य राग-द्वेष से मुक्त हो जाता है।
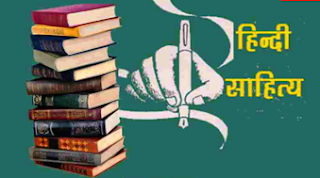
إرسال تعليق